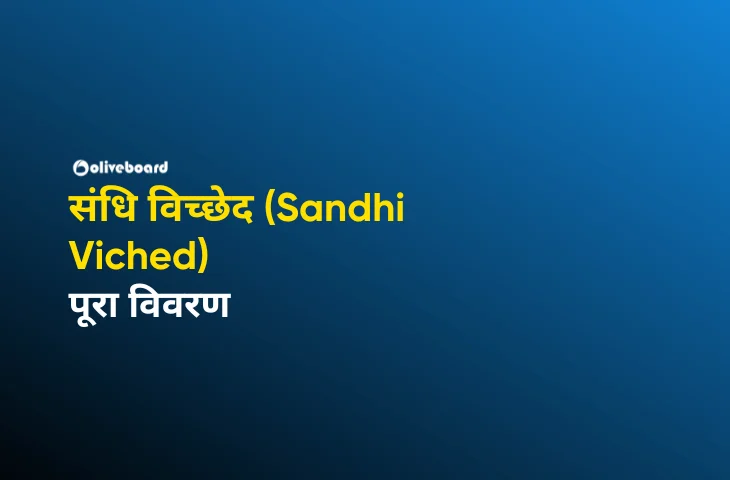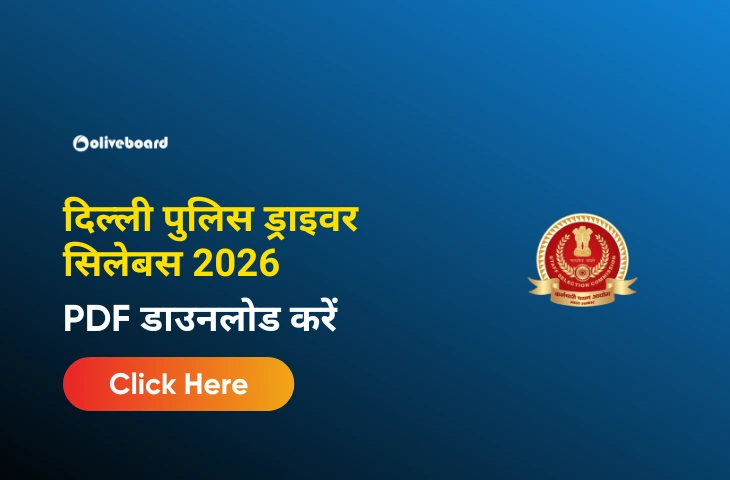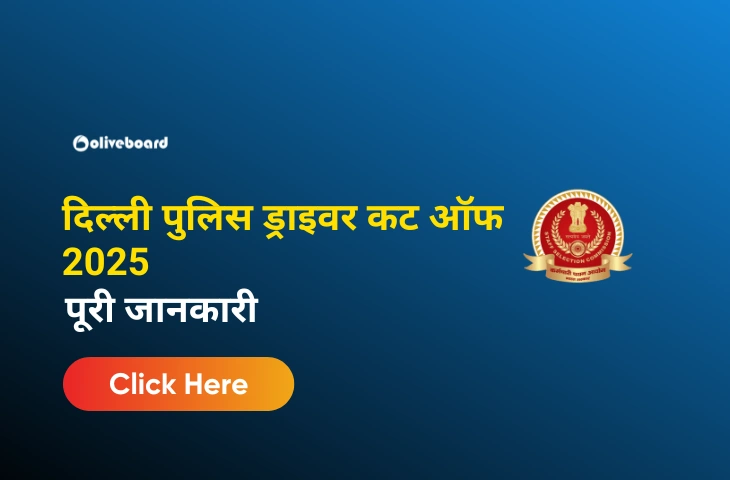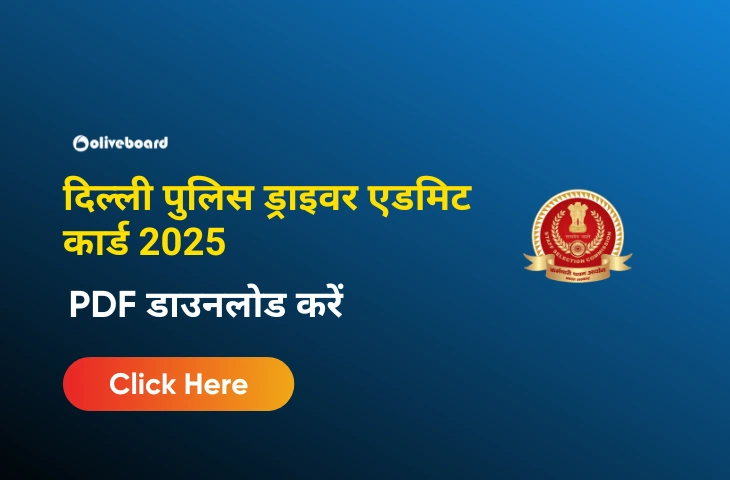संधि विच्छेद (Sandhi Viched) – हिंदी व्याकरण का पूर्ण मार्गदर्शन
भाषा विज्ञान में हिंदी वर्णमाला के विभिन्न वर्णों के समास्यता एवं विशेषताओं को समझने के लिए संधि विच्छेद एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। संधि विच्छेद का मूल उद्देश्य भाषा के शब्दों की उत्पत्ति और उनके वाक्यांतरण में आने वाले विभिन्न प्रकार के संधि समस्याओं को समझना है। हिंदी वर्णमाला में दो या दो से अधिक वर्णों के एक साथ मिलने से संधि बनती है और वाक्य रचना में संधि का बहुत महत्व होता है।
संधियों के प्रकार: संधियां तीन विभाजनों में होती हैं – स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि।
- स्वर संधि: स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से नए स्वर बनते हैं, जैसे दो वर्णों ‘अ’ और ‘इ’ के मिलने से ‘ए’ बन जाता है। यह संधि वाक्य में अधिक सुविधा प्रदान करती है और भाषा को समृद्ध बनाती है।
- व्यंजन संधि: व्यंजन संधि में दो व्यंजनों के मिलने से नए व्यंजन या स्वर का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए, दो व्यंजनों ‘स’ और ‘त’ के मिलने से ‘स्त’ बन जाता है।
- विसर्ग संधि: विसर्ग संधि में ‘ह’ या ‘ं’ विसर्ग के समानार्थी वर्ण के साथ विसर्जन होता है, जो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए, ‘रामः गच्छति’ में ‘ह’ विसर्ग के स्थान पर ‘गच्छति’ हो जाता है।
संधि क्या है?
संधि शब्द का अर्थ है – वर्णों का मिलन।
- परिभाषा: जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिलकर नया स्वर या व्यंजन उत्पन्न करते हैं, उसे संधि कहते हैं।
- महत्त्व:
- वाक्य संरचना को सरल और अर्थपूर्ण बनाना।
- उच्चारण में सुगमता और प्रवाह लाना।
- साहित्य और कविता में रचनात्मकता बढ़ाना।
संधियों के प्रकार
हिंदी व्याकरण में संधियों को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है:
- स्वर संधि (Vowel Sandhi)
- व्यंजन संधि (Consonant Sandhi)
- विसर्ग संधि (Visarga Sandhi)
स्वर संधि (Vowel Sandhi)
स्वर संधि वह संधि है जिसमें दो स्वर मिलकर नया स्वर बनाते हैं। स्वर संधि भाषा को मधुर, सरल और प्रवाहपूर्ण बनाती है।
स्वर संधि के प्रकार
(A) दीर्घ संधि (Dirgh Sandhi)
जब दो स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है।
- उदाहरण:
- अभीष्ट = अभि + इष्ट
- अन्नाभाव = अन्न + अभाव
- बुद्धीश = बुद्ध + ईश
- हिमालय = हिम + आलय
अभीष्ट (अभि+इष्ट), अन्नाभाव (अन्न+अभाव), बुद्धीश (बुद्ध+ईश), भारतीश्वर (भारती+ईश्वर), भानूदय (भानु+उदय), भोजनालय (भोजन+आलय), भूपरि (भू+उपरि), भूत्तम (भू+उत्तम), देवाधिवति (देव+अधिपति), धर्मार्थ (धर्म+अर्थ), गिरीश (गिरि+ईश), गिरीन्द्र (गिर+इन्द्र), गुणालय (गुण+आलय), हरीश (हरि+ईश), हिमालय (हिम+आलय), होतृकार (होतृ+ऋकार), जानकीश (जानकी+ईश), कवींद्र (कवि+इन्द्र), कपीश (कपि+ईश), कवीश (कवि+ईश), कटूक्ति (कटु+उक्ति), कामारि (काम+अरि), लक्ष्मीच्छा (लक्ष्मी+इच्छा), लघूक्ति (लघु+उक्ति), लघूर्मि (लघु+ऊर्मि), महींद्र (मही+इन्द्र), महीश (मही+ईश), महाशय (महा+शय), मंजूषा (मंजु+ऊषा), मातृणाण (मातृ+ऋणाम्), मुनीश्वर (मुनि+ईश्वर), मृत्यूपरांत (मृत्यु+उपरांत), नदीश (नदी+ईश), पुस्तकालय (पुस्तक+आलय), पृथ्वीश (पृथ्वी+ईश), पितृण (पितृ+ऋण), रघूत्तम (रघु+उत्तम), रतीश (रति+ईश), रजनीश (रजनी+ईश), स्वर्णावसर (स्वर्ण+अवसर), सूक्ति (सु+उक्ति), स्वयंभूदय (स्वयंभू+उदय), शरणार्थी (शरण+अर्थी), शिवालय (शिव+आलय), सिन्धूर्मि (सिन्धु+ऊर्मि), वधूत्सव (वधु+उत्सव), वधूर्मि (वधू+उर्मि), विद्यार्थी (विद्या+अर्थी), विद्यालय (विद्या+आलय), वधूल्लास (वधु+उल्लास), युवावस्था (युवा+अवस्था)।
(B) गुण संधि (Guna Sandhi)
जब स्वर ‘अ’ + ‘इ’ या ‘उ’ मिलकर गुण स्वर बनाते हैं।
- उदाहरण:
- चंद्रोदय = चन्द्र + उदय
- देवेंद्र = देव + इन्द्र
- गणेश = गण + ईश
चंद्रोदय (चन्द्र+उदय), दीर्घोपल (दीर्घ+ऊपल), देवेंद्र (देव+इन्द्र), देवेश (देव+ईश), देवर्षि (देव+ऋषि), गणेश (गण+ईश), गंगोर्मि (गंगा+ऊर्मि), जलोदय (जल+उदय), जलोर्मि (जल+ऊर्मि), खगेश (खग+ईश), लोकोपयोग (लोक+उपयोग), महोत्सव (महा+उत्सव), महोजस्वी (महा+ओजस्वी), महोर्जस्वी (महा+ऊर्जस्वी), महोर्मि (महा+उर्मि), महेश्वर (महा+ईश्वर), महेश (महा+ईश), महोपदेश (महा+उपदेश), महेंद्र (महा+इन्द्र), मृगेंद्र (मृग+इन्द्र), महर्षि (महा+ऋषि), नरेश (नर+ईश), नरेंद्र (नर+इन्द्र), परमोत्सव (परम+उत्सव), परोपकार (पर+उपकार), प्रेत (प्र+इत) परमेश्वर (परम+ईश्वर), रमेश (रमा+ईश), राजऋषि (राज+ऋषि), सप्तर्षि (सप्त+ऋषि), समुद्रोर्मि (समुद्र+ऊर्मि), सुरेंद्र (सुर+इन्द्र), सुरेश (सुर+ईश), सूर्योदय (सूर्य+उदय), उपेन्द्र (उप+इन्द्र)।
(C) वृद्धि संधि (Vriddhi Sandhi)
जब ‘अ’ + ‘ए/ऐ’ या ‘अ’ + ‘औ’ मिलकर वृद्धि स्वर बनता है।
- उदाहरण:
- एकैव = एक + एव
- महैश्वर्य = महा + ऐश्वर्य
- तत्रैव = तत्र + एव
एकदैव (एकदा+एव), एकैव (एक+एव), एकैक (एक+एक), दिनैक (दिन+एक), देवैश्वर्य (देव+ऐश्वर्य), धर्मैक्य (धर्म+ऐक्य), जलौस (जल+ओस), जलौक (जल+ओक), जलौषध (जल+औषध), महौज (महा+ओज), महौदार्य (महा+औदार्य), महौषध (महा+औषध), महैश्वर्य (महा+ऐश्वर्य), मतैक्य (मत+ऐक्य), नवैश्वर्य (नव+ऐश्वर्य), परमौज (परम+ओज), परमौषध (परम+औषध), परमौदार्य (परम+औदार्य), परमैश्वर्य (परम+एश्वर्य), सदैव (सदा+एव), सर्वदैव (सर्वदा+एव), तत्रैव (तत्र+एव), तथैव (तथा+एव), उष्णौदन (उष्ण+ओदन), वनौषधि (नव+औषधि), विश्वैक्य (विश्व+ऐक्य)।
(D) यण संधि (Yana Sandhi)
‘इ’ या ‘उ’ स्वर से यण स्वर का निर्माण।
- उदाहरण:
- अध्ययन = अधि + अयन
- अत्युत्तम = अति + उत्तम
- अन्वय = अनु + अय
अध्ययन (अधि+अयन), अन्वादेश (अनु+आदेश), अत्यंत (अति+अंत), अन्वय (अनु+अय), अन्वर्थ (अनु+अर्थ), अत्यर्थ (अति+अर्थ), अत्युक्ति (अति+उक्ति), अत्युत्तम (अति+उत्तम), अन्वय (अनु+अय), अन्विष्ट (अनु+इष्ट), अत्यधिक (अति+अधिक), अत्याचार (अति+आचार), अत्यूष्म (अति+ऊष्म), अन्वीक्षण (अनु+ईक्षण), अत्यावश्यक (अति+आवश्यक), भान्वागमन (भानु+आगमन), ऋत्वन्त (ऋतु+अन्त), देव्यागम (देवी+आगमन), देव्युक्ति (देवी+उक्ति), देव्यालय (देवी+आलय), देव्यैश्वर्य (देवी+ऐश्वर्य), देव्योज (देवी+ओज), देव्यौदार्य (देवी+औदार्य),देव्यंग(देवी+अंग), धात्विक (धातु+इक), गुर्वौदन (गुरु+ओदन), गुर्वौदार्य (गुरु+औदार्य), इत्यादि (इति+आदि), मन्वन्तर (मनु+अन्तर), मध्वरि (मधु+अरि), मध्वालय (मधु+आलय), मात्रार्थ (मातृ+अर्थ), न्यून (नि+ऊन), नद्यर्पण (नदी+अर्पण), नद्यूर्मि (नदी+ऊर्मि), प्रत्युत्तर (प्रति+उत्तर), प्रत्येक (प्रति+एक), प्रत्युपकार (प्रति+उपकार), प्रत्यूष (प्रति+ऊष), पित्राज्ञा (पितृ+आज्ञा), रीत्यानुसार (रीति+अनुसार), स्वागत (सु+आगत), सख्यागम (सखी+आगम), सख्युचित (सखी+उचित), सरस्वत्याराधना (सरस्वती+आराधना), उपर्युक्त (उपरि+उक्त), वध्वर्थ (वधू+अर्थ), वध्वागमन (वधू+आगमन), वाण्यूर्मि (वाणि+ऊर्मि), वध्विष्ट (वधू+इष्ट), वध्वीर्ष्या (वधू+ईर्ष्या), यद्यपि (यदि+अपि)।
(E) अयादि संधि (Ayadi Sandhi)
विशेष स्वर संधि जो ऊपर की श्रेणियों में न आती हों।
- उदाहरण:
- अन्वेषण = अनु + एषण
- नायक = नै + अक
- मध्वोदन = मधु + ओदन
अन्वेषण (अनु+एषण), भवन (भो+अन), भ्रात्रोक (भ्रातृ+ओक), भ्रात्रेषणा (भ्रातृ+एषणा), चयन (चे+अन), गायक (गै+अक), गायन (गै+अन), गवीश (गो+ईश), गवन (गो+अन), गुर्वोदार्य (गुरु+औदार्य), मध्वोदन (मधु+ओदन), मध्वौषध (मधु+औषध), मात्रादेश (मातृ+आदेश), मात्रानन्द (मातृ+आनन्द), मात्रंग (मातृ+अंग), नयन (ने+अन), नायक (नै+अक), पवित्र (पो+इत्र), पवन (पो+अन), पावक (पौ+अक), पावन (पौ+अन), पित्रादेश (पितृ+आदेश), पित्रनुदेश (पित्र+अनुदेश), पित्रनुमति (पितृ+अनुमति), पावन (पौ+अन), पावक (पौ+अक), रवीश (रवि+ईश), सायक (सै+अक), शयन (शे+अन), वध्वंग (वधू+अंग), वध्वादेश (वधू+आदेश), वध्वेषण (वधू+एषण), वध्विष्ट (वधू+इष्ट), वध्वर्थ (वधू+अर्थ), श्रवण (श्रो+अन), श्रावन (श्रौ+अन)।
व्यंजन संधि (Consonant Sandhi)
व्यंजन संधि में दो व्यंजन मिलकर नया व्यंजन या स्वर उत्पन्न करते हैं।
- उदाहरण:
- अभी + सेक = अभिषेक
- वायु + आकार = वायुआकार
- स्त + रियों = स्त्रीयों
व्यंजन संधि वाक्य संरचना और उच्चारण में सहूलियत लाती है।
विसर्ग संधि (Visarga Sandhi)
विसर्ग संधि वह संधि है जिसमें विसर्ग (ः) और अन्य वर्णों के मेल से नया स्वर या व्यंजन बनता है।
- उदाहरण:
- मन + अनुकूल = मनोनुकूल
- निः + अक्षर = निरक्षर
- प्रातः + काल = प्रातःकाल
विसर्ग संधि के नियम
| नियम | उदाहरण |
| विसर्ग + च/छ = श् | निः + चल = निश्चल |
| विसर्ग + ट/ठ = टंकार | धनुः + टंकार = धनुष्टकार |
| विसर्ग + त/थ = स् | निः + तेजः = निस्तेज |
| विसर्ग + क/ख/प = क/प | निः + कपट = निष्कपट / दुः + ख = दुःख |
| विसर्ग + श/स = श/स | दुः + शासन = दुःशासन |
विसर्ग ज्यों का त्यों या ‘स’ में बदल सकता है।
संधि विच्छेद क्यों महत्वपूर्ण है?
संधि विच्छेद का महत्व इस प्रकार है:
- भाषा की शुद्धता: सही संधि विच्छेद से शब्दों का उच्चारण और अर्थ स्पष्ट रहता है।
- व्याकरण में दक्षता: परीक्षा, लेखन और पाठ में सही शब्द चयन।
- साहित्यिक उपयोग: कविता, गद्य और संस्कृत ग्रंथों में संधियों का सही प्रयोग आवश्यक।
संधि विच्छेद के उदाहरण
संधि विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
स्वर संधि
- अभीष्ट = अभि + इष्ट
- चंद्रोदय = चन्द्र + उदय
- एकैव = एक + एव
व्यंजन संधि
- अभिषेक = अभी + सेक
- वायुआकार = वायु + आकार
विसर्ग संधि
- निश्चल = निः + चल
- प्रातःकाल = प्रातः + काल
- निरक्षर = निः + अक्षर
अभ्यास के लिए सुझाव
- शब्दों के संधि विच्छेद को तालिका में लिखकर याद करें।
- सरकारी परीक्षा के लिए स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के उदाहरण याद रखें।
- कविताओं और ग्रंथों में प्रयोग देखकर अभ्यास बढ़ाएँ।
प्रश्न
प्रश्न 1: संधि विच्छेद क्या होता है?
उत्तर: संधि विच्छेद एक हिंदी व्याकरणिक नियम है जिसमें वर्णों या शब्दों के मेल के आधार पर उनमें विकार या परिवर्तन का होना है। यह विकार वाक्य रचना और अर्थ में परिवर्तन को उत्पन्न करता है और हिंदी भाषा में शब्दों का सही उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 2: संधि विच्छेद का क्या उद्देश्य होता है?
उत्तर: संधि विच्छेद का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति और उनके वाक्यांतरण में आने वाले विभिन्न प्रकार के संधि समस्याओं को समझना है। इससे शब्दावली में वृद्धि होती है और भाषा के संरचनात्मक दृष्टिकोन से छात्रों को अधिक अवधारणा प्राप्त होती है। संधि विच्छेद का अध्ययन हिंदी भाषा के सही उपयोग के लिए आवश्यक है और इससे भाषा के शैलीशास्त्रीय रूप से उन्नति होती है।
- राक्षस का पर्यायवाची शब्द | Rakshas Ka Paryayvachi Shabd
- आसमान का पर्यायवाची शब्द | Aasman Ka Paryayvachi Shabd
- देवता का पर्यायवाची शब्द | Devta ka Paryayvachi Shabd
- Surya Ka Paryayvachi Shabd |सूर्य का पर्यायवाची शब्द
- Ghar Ka Paryayvachi shabd | घर का पर्यायवाची शब्द
- Guru Ka Paryayvachi Shabd | गुरु के पर्यायवाची शब्द

नमस्ते, मैं अदिति हूँ। मैं Oliveboard में Content Writer के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 4 वर्षों से मैं परीक्षा से जुड़ी जानकारी को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए छात्रों को आसान और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करना है। मैं नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और परीक्षा से संबंधित अपडेट को सरल शब्दों में समझाती हूँ, साथ ही स्टडी प्लान और विषयवार रणनीतियाँ तैयार करती हूँ। मेरा लक्ष्य है कि कामकाजी पेशेवर अपने नौकरी और परीक्षा तैयारी के बीच संतुलन बना सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें ।