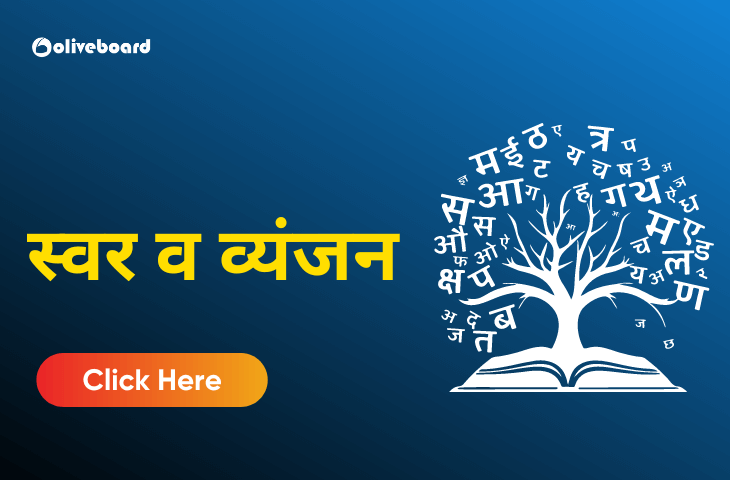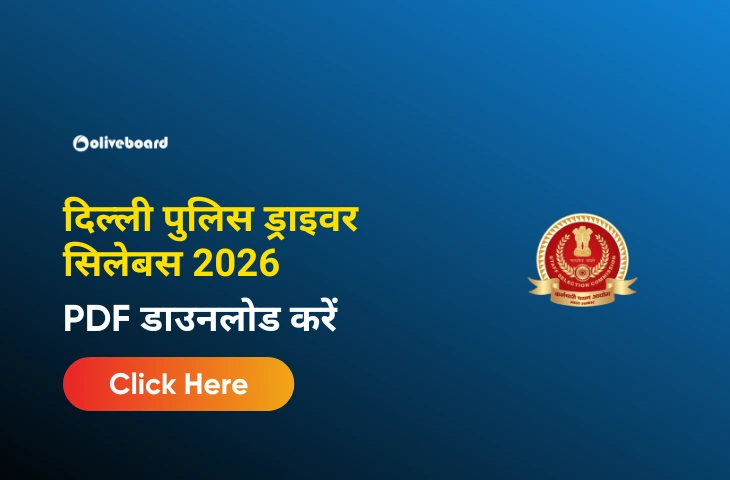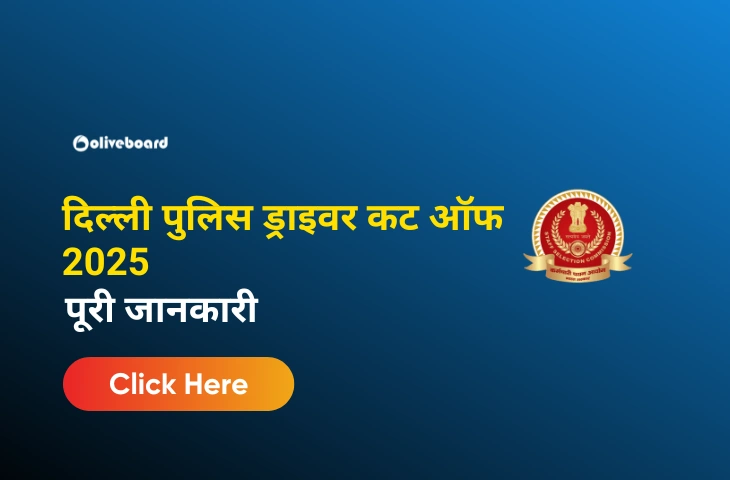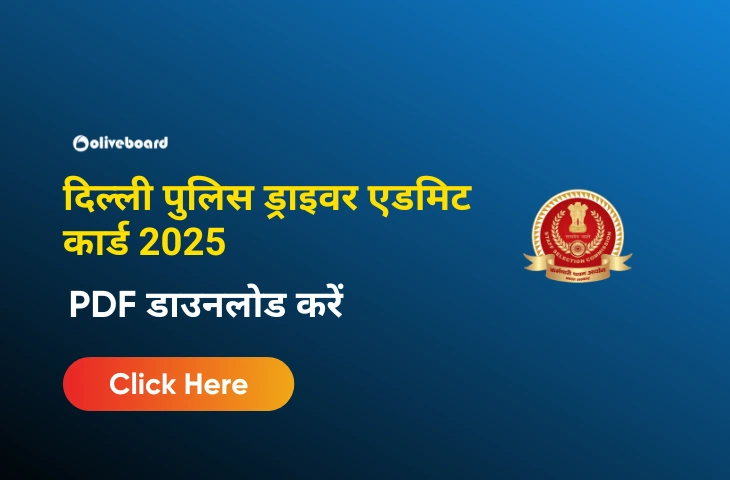स्वर और व्यंजन (swar and vyanjan )
स्वर और व्यंजन हिन्दी भाषा के ध्वनि तत्व हैं जो व्यक्ति को भाषा का सही ढंग से उच्चारण करने में सहायक होते हैं। ये ध्वनि तत्व भाषा की सुंदरता और सांविदानिक संरचना को बढ़ावा देते हैं और भाषा को समृद्धि देते हैं।
स्वर:
स्वर ध्वनि तत्व हैं जो बिना किसी रुकावट के निर्मित होते हैं। इनमें वायुमंडल का बहुतम निर्माण होता है और वे बिना किसी वर्ण वृद्धि के स्वतंत्र रूप से निकलते हैं। हिन्दी में कुल 13 स्वर होते हैं, जो निम्नलिखित हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, ऋ।
इन स्वरों में हर एक का अपना विशेष ढंग होता है और इन्हें सही ढंग से उच्चारित करने के लिए वक्ता को उचित साथ की आवश्यकता होती है। स्वरों का सही प्रयोग न केवल भाषा को सुंदर बनाए रखता है बल्कि इससे शब्दों का अच्छा अर्थ भी सामने आता है।
व्यंजन:
व्यंजन ध्वनि तत्व हैं जो वायुमंडल में किसी प्रकार की रुकावट के साथ उत्पन्न होते हैं। इन्हें उच्चारित करते समय वयंजन क्षेत्र में कोई न कोई रुकावट आती है, जिससे ध्वनि निर्माण होती है।
हिन्दी में कुल 25 व्यंजन होते हैं, जो निम्नलिखित हैं: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
व्यंजनों का सही उच्चारण और उनकी सही स्थिति भाषा को शुद्ध और सुंदर बनाए रखता है। इन्हें सही रूप से प्रयोग करने से शब्दों का सही अर्थ आता है और वाक्य गति सही होती है। व्यंजनों की मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें उच्चारित करते समय वक्ता को अपनी जिह्वा या ऊपरी होंठों का सही स्थान पर ले जाना होता है।
स्वर और व्यंजन का महत्व:
स्वर और व्यंजन भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें सही ढंग से उच्चारित करने से एक व्यक्ति की भाषा संवेदनशीलता बढ़ती है और उसकी विचारशीलता में सुधार होता है।
अगर किसी भी भाषा में स्वर और व्यंजन सही नहीं होंगे, तो वह भाषा अव्यावसायिक और अस्पष्ट हो जाएगी।
स्वरों और व्यंजनों का मिलन भाषा को रंगीन बनाता है और उसे विभिन्न शैलियों में व्यक्त करने में सहारा प्रदान करता है। इन ध्वनि तत्वों का सही समांजस्य और समन्वय होना चाहिए ताकि भाषा का संवेदनशीलता से भरपूर हो सके और व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को सही ढंग से अभिव्यक्त कर सके।
स्वर और व्यंजनों का सही उपयोग न केवल व्यक्ति को सही रूप से बोलने में मदद करता है, बल्कि इससे उसकी लेखनी, पठनी, और सुनने की क्षमताएं भी विकसित होती हैं। यह ध्वनि तत्व भाषा को जीवंत बनाए रखते हैं और समृद्धि में सहायक होते हैं।
उच्चारण के लिए लगने वाले वक्त के आधार पर स्वर कुल तीन प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं।
हृस्व स्वर (एक मात्रिक स्वर)
हृस्व स्वर वे होते हैं जो एक मात्रा के लिए लगते हैं। इनमें शोर्ट ध्वनि होती है और उन्हें तेजी से उच्चारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अ, इ, उ, ए आदि हृस्व स्वरों की उदाहरण हैं।
| अ | इ | उ | ऋ |
दीर्घ स्वर (द्विमात्रिक स्वर)
दीर्घ स्वर वे होते हैं जो दो मात्राओं के लिए लगते हैं। इनमें धीर्घ ध्वनि होती है और उन्हें धीमे गति से उच्चारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आ, ई, ऊ, ओ आदि दीर्घ स्वरों की उदाहरण हैं।
| आ | ई | ऊ | ए | ऐ | ओ | औ |
प्लुत स्वर (त्रिमात्रिक स्वर)
प्लुत स्वर वे होते हैं जो तीन मात्राओं के लिए लगते हैं। इनमें ध्वनि की और बढ़ावा होता है और उन्हें धीमे गति से उच्चारित किया जाता है। इसमें अधिक समय का लगता है और ध्वनि को विस्तारपूर्वक सुनाया जाता है। उदाहरण के लिए, अं, अः, ऋ आदि प्लुत स्वरों की उदाहरण हैं।
स्वर की मात्राएँ — Swar Ki Matra
| अक्षर | मात्राएँ | शब्द |
|---|---|---|
| अ | – | कम |
| आ | ा | काम |
| इ | ि | किसलय |
| ई | ी | खीर |
| उ | ु | गुलाब |
| ऊ | ू | भूल |
| ऋ | ृ | तृण |
| ए | े | केश |
| ऐ | ै | है |
| ओ | ो | चोर |
| औ | ौ | चौखट |
व्यंजन भाषा के ध्वनि तत्व हैं जो वायुमंडल में किसी प्रकार की रुकावट के साथ उत्पन्न होते हैं। इन्हें उच्चारित करते समय वयंजन क्षेत्र में कोई न कोई रुकावट आती है, जिससे ध्वनि निर्माण होती है। हिन्दी में कुल 25 व्यंजन होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:
कवर्ग (वायुस्थ)
इन्हें कवर्ग कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण कवर्ग (वायुमंडल) से होता है। इनमें से च, छ, ज, झ, ञ व्यंजन शामिल हैं।
तालवायु (नासिक)
इनमें नाक से उच्चारित होने वाले व्यंजन शामिल हैं और इसलिए इन्हें तालवायु व्यंजन कहा जाता है। इस श्रेणी में अं, अः, ऋ व्यंजन शामिल हैं।
मूर्धन्य (मूर्धन)
इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण मस्तिष्क (मूर्धन) से होता है। इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण व्यंजन शामिल हैं।
दंत्य (दंत)
इनमें उच्चारण दंत से होता है और इसलिए इन्हें दंत्य व्यंजन कहा जाता है। इस श्रेणी में त, थ, द, ध, न व्यंजन शामिल हैं।
ओष्ठ्य (ओष्ठ)
इन्हें उच्चारण ओष्ठ से होता है और इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। इसमें प, फ, ब, भ, म व्यंजन शामिल हैं।
इन व्यंजनों का सही और सुंदर उच्चारण भाषा को सांविदानिक और सुंदर बनाए रखता है और विचारशीलता में सुधार करता है। व्यंजनों का सही रूप से प्रयोग न केवल उच्चारण को सुधारता है बल्कि इससे शब्दों का सही अर्थ भी सामने आता है और वाक्य गति सही होती है। इसके बिना भाषा संवेदनशीलता और सुंदरता में कमी हो जाती है।

नमस्ते, मैं अदिति हूँ। मैं Oliveboard में Content Writer के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 4 वर्षों से मैं परीक्षा से जुड़ी जानकारी को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए छात्रों को आसान और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करना है। मैं नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड और परीक्षा से संबंधित अपडेट को सरल शब्दों में समझाती हूँ, साथ ही स्टडी प्लान और विषयवार रणनीतियाँ तैयार करती हूँ। मेरा लक्ष्य है कि कामकाजी पेशेवर अपने नौकरी और परीक्षा तैयारी के बीच संतुलन बना सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें ।